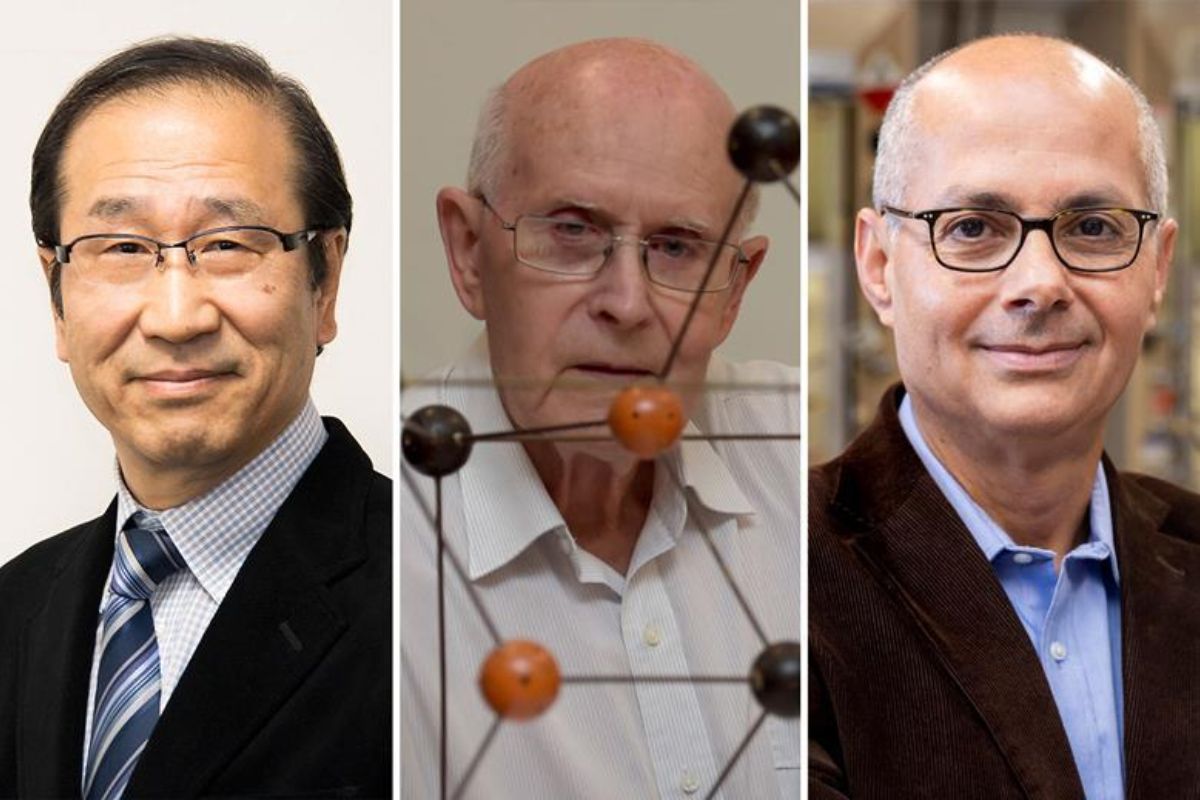मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के पीपलिया मीर गांव में रहने वाले मनोहर मेवाड़ा देश के उन 65 लाख लोगों में से एक हैं जिन्हें स्वामित्व योजना के तहत गांव में स्थित अपने घर का संपत्ति कार्ड मिला है। इस संपत्ति कार्ड की मदद से मनोहर मेवाड़ा को बैंक से 10 लाख का लोन मिला है। मनोहर के लिए यह पहले संभव नहीं था, क्योंकि उनके पास अपनी ही ज़मीन के मालिकाना हक़ के कागज़ नहीं थे। बैंक से मिले लोन की मदद से मनोहर मेवाड़ा ने 5 गाय और एक भैंस लेकर अपना डेयरी फार्म शुरु किया है। इससे उन्हें हर माह 30 हज़ार रुपए की आमदनी होती है। इस एक्सप्लेनर में हम समझने का प्रयास करेंगे की स्वामित्व योजना क्या है और इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाली आबादी को किस प्रकार लाभ हो सकता है।
आज भी अक्सर हमें ऐसी खबरें और घटनाएं देखने सुनने को मिलती हैं कि सड़क के लिए किसी का घर उजड़ा लेकिन उसे उसका मुआवजा नहीं मिला। इसकी वजह थी अधिकांश ग्रामीण आबादी के पास अपनी ज़मीन का मालिकाना हक न होना। इसी समस्या को केंद्र में रखते हुए भारत सरकार स्वामित्व योजना लेकर आई। इस योजना का मकसद ग्रामीण आबादी का सर्वे करके उन्हें उनके निवास का मालिकाना हक देना है।
भारत के ग्रामीण अंचलों में भू-संपत्ति से जुड़ी समस्याएं
लंबे समय तक, भारत में ग्रामीण आबादी वाले क्षेत्रों में व्यवस्थित और कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त संपत्ति रिकॉर्ड का अभाव था। एक रिपोर्ट के मुताबिक कृषि भूमि में अक्सर अधिकारों का औपचारिक रिकॉर्ड होता था। लेकिन गांवों के भीतर आवासीय क्षेत्र काफी हद तक अनिर्दिष्ट थे या पुराने और गलत रिकॉर्ड थे। संपत्ति के स्पष्ट स्वामित्व की कमी के कारण कई गंभीर समस्याएं पैदा हुईं। स्पष्ट सीमांकन और स्वामित्व अभिलेखों की अनुपस्थिति के परिणामस्वरूप अक्सर संपत्ति की सीमाओं और विरासत पर विवाद होते थे, जिससे सामाजिक तनाव और गांवों के भीतर लंबे समय तक कानूनी लड़ाई होती थी।
अपनी जमीन के औपचारिक दस्तावेज न होने की वजह से ग्रामीण निवासी औपचारिक संस्थानों से ऋण और अन्य वित्तीय लाभ प्राप्त करने के लिए अपनी आवासीय संपत्तियों का उपयोग कोलैट्रल के रूप में नहीं कर सकते थे। इससे उनकी आजीविका में निवेश करने, अपने घरों में सुधार करने या तत्काल वित्तीय जरूरतों को पूरा करने की क्षमता बाधित और आर्थिक प्रगति बाधित होती थी। सटीक स्थानिक आंकड़ों और संपत्ति मानचित्रों की कमी ने अन्य सरकारी एजेंसियों के लिए बुनियादी ढांचे के विकास, नागरिक सुविधाओं के प्रावधान और समग्र ग्राम विकास के लिए प्रभावी योजना बनाना मुश्किल बना दिया था।

इसके अलावा जिन राज्यों में आबादी वाले क्षेत्रों पर संपत्ति कर लगाया जा सकता था, वहां स्पष्ट स्वामित्व रिकॉर्ड और संपत्ति की सीमाओं के अभाव ने ग्राम पंचायतों के लिए कर निर्धारण और संग्रह को अत्यधिक चुनौतीपूर्ण बना दिया था। इसने उनके अपने राजस्व के स्रोत और स्थानीय विकास कार्यों को निधि देने की उनकी क्षमता को सीमित कर दिया था।
अंततः रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि ग्रामीण क्षेत्रों में पारंपरिक तरीके से होने वाले सर्वे में अशुध्दियों की काफी गुंजाईश रहती थी। ये सर्वे कई बार एक क्षेत्र विशेष को व्यापक रूप से कवर भी नहीं कर पाते थे। इन्हीं चुनौतियों को ध्यान में रख कर स्वामित्व योजना लाई गई, जिसमें तकनीक आधारित ड्रोन बेस्ड सर्वे का सहारा लिया गया।
स्वामित्व योजना की प्रक्रिया
स्वामित्व योजना एक सहयोगी प्रयास है जिसमें नोडल मंत्रालय के रूप में पंचायती राज मंत्रालय, प्रौद्योगिकी कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में भारतीय सर्वेक्षण (एसओआई), राज्य राजस्व विभाग, राज्य पंचायती राज विभाग, स्थानीय जिला प्राधिकरण, ग्राम पंचायत और संपत्ति के मालिक शामिल होते हैं। सबसे पहले पंचायती राज मंत्रालय और राज्यों के बीच एक एमओयू साझा होता है। इसके एसओआई राज्य सरकार को परामर्श देता है। इस परामर्श के आधार पर गांवो की पहचान की जाती है और सर्वे की रूपरेखा तैयार की जाती है। इसके अलावा राज्य में लागू राजस्व और भू-संपत्ति संबंधी नियम कानूनों में आवश्यक संशोधन भी किये जाते हैं, ताकि जारी होने वाले संपत्ति कार्डों की कानूनी वैधता सुनिश्चित हो सके।
इन गतिविधियों के बाद राज्य में सर्वे की प्रक्रिया शुरू की जाती है। सर्वे के लिए सबसे पहले अगर संभावना हो तो, सीओआरएस (Continuously Operating Reference Station) स्थापित किये जाते हैं। ये एक प्रकार के जीपीएस रेफरेंस स्टेशन होते हैं, जो सटीक और विश्वशनीय नतीजे निकालने में मदद करते हैं।
इसके बाद जिले के कलेक्टर सर्वे की घोषणा करते हैं। राजस्व विभाग के कर्मचारी, आमतौर पर पटवारी गांवों में जाकर प्राथमिक सर्वे करते हैं। इसके बाद जमीनों को चिन्हित किया जाता है और चूने से सीमाएं बनाकर जमीन की डिमार्किंग की जाती है। डिमार्किंग के आधार पर ड्रोन की मदद से इन सभी जमीनों हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें ली जाती हैं और नक़्शे तैयार किये जाते हैं।
ड्रोन द्वारा एकत्र किए गए रॉ डेटा को भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रोसेस किया जाता है। इस डाटा को मानचित्रों के साथ ऑर्थो-रेक्टिफाइड इमेज (ओआरआई) और एक जीआईएस डेटाबेस तैयार करने के लिए उपयोग किया जाता है। इस डिजिटल डेटा में संपत्ति की सीमाएं, आयाम और अन्य स्थानिक जानकारी शामिल होती हैं। डेटाबेस तैयार हो जाने के बाद, जानकारियों का ग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाता है। इस प्रक्रिया में ग्राम पंचायतों की मदद ली जाती है।
ग्राउंड वेरिफिकेशन के बाद जरूरी सुधार किये जाते हैं। इसके बाद भारतीय सर्वेक्षण संस्थान द्वारा बनाए गए ‘सारथी ऍप’ की मदद से इन मानचित्रों में अपडेशन किये जाते हैं। इसके बाद इन सभी जानकरियों की राजस्व महकमे, पंचायत इत्यादि के माध्यम से जांच की जाती है। अगर मौजूदा रिकॉर्ड और कब्जे से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसका भी निपटारा किया जाता है।
अंततः मानचित्र, डेटाबेस, और राज्य के कानूनों को संदर्भ में रखते हुए स्वामित्व कार्ड बनाए और प्रदान किये जाते हैं। इन संपत्ति कार्डों में संपत्ति के मालिक का विवरण, संपत्ति के आयाम और संपत्ति की एक यूनीक आईडी होती है, और इसमें एक क्यू. आर. कोड भी शामिल होता है।

हाल ही में ग्राउंड रिपोर्ट ने सीहोर के ही भाउखेड़ी गांव में सड़क के निर्माण के लिए सुरेश जैन के घर को अवैध बताकर तोड़ने की खबर प्रकाशित की थी। सुरेश जैन का परिवार वर्षों से भाउखेड़ी गांव में रह रहा था। लेकिन जिस घर में सुरेश जैन रह रहे थे उसकी रजिस्ट्री या कोई कागज़ उनके पास नहीं था, ऐसे में उन्हें कोई मुआवज़ा नहीं दिया गया। उम्मीद है कि स्वामित्व योजना से जो ग्रामीणों को उनके घर का नक्शा और उस पर हक दिया जा रहा है, इसकी मदद से वे भविष्य में अपने प्रॉपर्टी पर हक साबित कर पाएंगे।
भारत में स्वतंत्र पर्यावरण पत्रकारिता को जारी रखने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट को आर्थिक सहयोग करें।
यह भी पढ़ें
40 फीसदी बिगड़े वन निजी कंपनियों को देने से आदिवासियों का क्या होगा?
आदिवासी बनाम जनजातीय विभाग: ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन ही होगी सुनवाई
“जंगल की ज़मीन सरकार की संपत्ति नहीं” किस अधिकार से निजी कंपनियों को दी जाएगी लीज़?
बुंदेलखंड के गांवों में जल संचय की गुहार लगाती जल सहेलियों की टोली
पर्यावरण से जुड़ी खबरों के लिए आप ग्राउंड रिपोर्ट को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब और वॉट्सएप पर फॉलो कर सकते हैं। अगर आप हमारा साप्ताहिक न्यूज़लेटर अपने ईमेल पर पाना चाहते हैं तो यहां क्लिक करें।
पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन से जुड़ी जटिल शब्दावली सरल भाषा में समझने के लिए पढ़िए हमारी क्लाईमेट ग्लॉसरी।